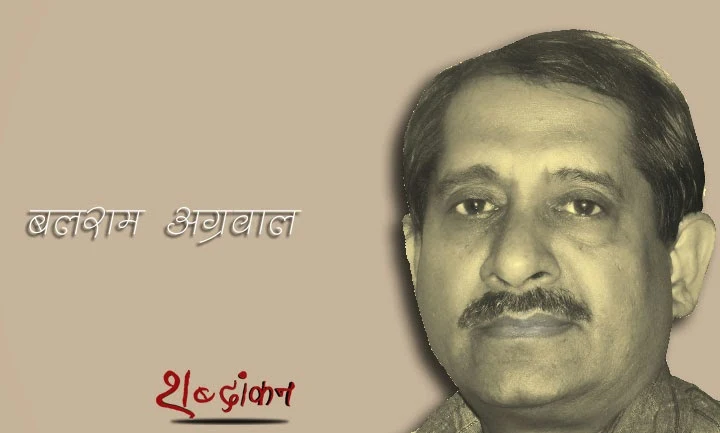
बादल बारिश भीजनहार
-बलराम अग्रवाल
बाबा राजराजेश्वर महाराज का, सोमनाथ पर मुहम्मद गज़नवी के हमलों वाले समय जितना पुराना मंदिर।
अब से चालीस साल पहले इसके चारों ओर की खुली जगह हमारा खेल-प्रांगण होती थी। कभी हम फुटबॉल खेलते थे, कभी क्रिकेट, कभी कबड्डी तो कभी गेंद-तड़ी। चोर-सिपाही के छापामार खेल में इसके अहाते हमें छिपने और भाग जाने में खासी मदद करते थे। घने पेड़ों में हम बंदरों की तरह चढ़-उतर जाने के अभ्यस्त थे और चिडि़यों की तरह चहकने के भी। अब, चालीस साल बाद आया हूँ तो चारों ओर की जगह अलग-अलग समुदाय के लोगों द्वारा हथियाई या बेची-खरीदी जा चुकी है। मंदिर के मुख्य प्रांगण को खत्म करके साईं बाबा, शनिदेव, मनसा देवी, संतोषी माता आदि कुछ और मूर्तियों की स्थापना कर दी गई है। लम्बे समय तक मंदिर के ट्रस्टी रहे भ्रष्ट एडवोकेट शंभू दयाल की भी एक मूर्ति मंदिर के प्रांगण में स्थापित हो गई है। ट्रस्ट पर अब उनके बेटों ने कब्जा कर लिया है। बड़े वाला एक दबंग राजनीतिक दल का प्रांतीय अध्यक्ष है और छोटे वाला एस.डी.एम.।
मेरी स्मृति में मंदिर का वह पुराना ही रूप रहने के कारण इस नए रूप पर श्रद्धा उभर नहीं पा रही है। जैसे-तैसे मत्था टेककर बाहर आया तो वयोवृद्ध पुजारी जगदीश भारती जी से भेंट हो गई। हमारे बचपन में वे अधेड़ उम्र में भी खासे दर्शनीय जवान थे और परहितकारी भी। कोमल हृदय इतने कि एक खूबसूरत विधवा को जात-पात का भेद किए बिना सहारा देकर अपनी दूसरी पत्नी के रूप में रख लिया था। लोगों ने कानाफूसी तो बहुत की, विरोध लेशमात्रा भी नहीं किया। थोड़ी-बहुत रार उनकी ब्याहता पत्नी ने ज़रूर की थी लेकिन वह बेअसर रही। कुछ माह बाद विधवा में गर्भ धारण के लक्षण दिखाई दिए तो उस बेचारी के भीतर भी ममत्व जाग उठा। बेटी की उम्र की ही थी। माँ की तरह उसकी देखभाल शुरू कर दी और खुद को बेसहारा होने से बचा लिया। जगदीश भारती को हम ताऊ जी कहा करते थे। याद दिलाया तो पहचान गये। पुरानी बातें बताने लगे। कोई बात पता नहीं कहाँ से चली थी और चलते-चलते कब ‘नेमचंद उर्फ़ नेमा’ का जिक्र छिड़ गया, पता ही नहीं चला। फिर तो बचपन में उतरते हुए नेमचंद की कुछेक बातें मैंने भी सुनाईं; लेकिन एक बात जो उन्होंने सुनाई, वह मुझे अमूल्य निधि-सी लगी।
साधू ऐसा चाहिए
अब तो गली मोहल्लों में रामलीलाओं और रासलीलाओं के मंचित होने का ज़माना लद ही चुका है। असलियत यह है कि अब मोहल्लों का ही ज़माना लद चुका है। उधर, जब से रामानंद सागर ने रामायण टी.वी. सीरियल बनाया है, तब से छोटे-मोटे रामलीला समूह तो खत्म ही हो गये हैं। बड़ी मछलियाँ कैसे छोटी मछलियों को खा जाती हैं, यह उसका नायाब नमूना है। बड़ी कालोनियों और टाउनशिप्स की रेजीडेंट वेलफेअर कमेटियाँ कुछ फंड इकट्ठा करके उस सीरियल की सीडीज़, प्रोजेक्टर और परदा आदि खरीद लाती हैं और सालों-साल के लिए बेफिक्र हो जाती हैं। रामलीला समूह वाले बहुत मुँह फाड़ने लगे थे; तरह-तरह के नखरे अलग। कम से कम पन्द्रह दिनों के लिए घर-दफ्तर सब छूट ही जाता था उनके चक्कर में। आज यह लाओ जी, कल वह लाओ जी। पूरी करनी पड़ती थी उनकी उल्टी-सीधी हर माँग। पूरे ग्रुप में एक-दो बंदा तो ऐसा उजड्ड निकल ही आता था जो न अपने मैनेजर की सुनता था न आर.डब्लू.ए. के सचिव की। अब कोई झंझट नहीं। न ही किसी उजड्ड को सम्हालने का सिरदर्द। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से लेकर रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी तक, सब तब तक चुपचाप सीडीज़ में सोए रहते हैं जब तक कि उन्हें उठाने को बटन न पुश कर दिया जाए।
आपको तो याद ही होगा कि हमारे ज़माने में छोटेलाल का रामलीला समूह इलाके भर में मशहूर था। उस समूह का राम एकदम राम लगता था और लक्ष्मण एकदम लक्ष्मण। दोनों लड़के चौदह-पंद्रह साल से ज़्यादा उम्र के नहीं रहे होंगे। क्या संवाद बोलते थे...ग़ज़ब। किसी से भी बात करते समय राम के मुँह से जैसे फूल झरते थे और क्रुद्ध लक्ष्मण के पोर-पोर से अंगार। उस समूह का परशुराम जितना भयंकर लगता था, उससे कहीं ज्यादा भयंकर लगता था रावण। दशरथ का रोल करने वाला खुद छोटेलाल होता था। राम के वियोग में वह ऐसे तड़पता था कि देखने वालों का कलेजा मुँह को आ जाता था। इन सबसे ऊपर था नानक नाम का कलाकार। वह आल राउण्डर था। कभी भरत का किरदार निभाता था तो कभी मारीच का; कभी जटायु बनकर रावण से लड़ता दिखाई देता था तो कभी नर्तकी बनकर रावण के दरबार में नाचता दिखाई देता था। उसकी खूबी यह भी थी कि वह नचनिया बड़े ग़ज़ब का था। सजी-धजी शूर्पणखा बनकर जब वह पंचवटी में बैठे राम-सीता और लक्ष्मण के समक्ष जाता था तो दर्शकों को बाँधकर रख देता था। लक्ष्मण को रिझाने के लिए शूर्पणखा बना वह गाता था—मैं तो छोड़ आई लंका का राज लछमन तेरे लिए...। कैसी-कैसी लुभावनी अदाएँ वह लक्ष्मण के सामने पेश करता था—हे भगवान! लोगों की साँसें रोक देता था। शूर्पणखा बना हो या रावण के राज-दरबार की नर्तकी, नाचने के लिए जब भी वह मंच पर आता, लहँगा पहनकर आता। हजार घूमों वाला राजस्थानी लहँगा। आगे छातियों तक उतरा घूँघट होता था और पीछे नितम्बों पर काले साँप-सी लहराती लम्बी चोटी। बैरी कजरा रे, हाय-हाय बैरी कजरा, मैं कबहुँ न सारउंगी तोय, बैरी कजरा... यह ऐसा गीत था जिस पर उसका नाच देखने के लिए दूर-दराज की बहू-बेटियाँ भी आती थीं। नाचते-नाचते एक खास अंदाज में लहँगे को आगे से पूरा उठाकर वह इस तरह ज़मीन पर बैठता था कि दूर तक बैठे मर्दों के दिल भी उसके साथ बैठ जाते थे। औरतें और लड़कियाँ सोचती थीं कि हाय, इस नानक जैसा नाचना हमें क्यों नहीं आया। वक्त आने पर अपने चहेतों को लुभाने की गरज़ से उन दिनों, किशोर उम्र के कितने ही लड़के-लड़कियाँ घर के भीतरी कमरों में बन्द होकर उसके स्टेप्स का अभ्यास करते थे।
ठेठ लोक शैली की अपनी नृत्यकला के बल पर नानक इलाके भर के लोगों के दिल पर राज करता था। नाचना नानक का शौक था; लेकिन उसको नचाना छोटेलाल की मजबूरी होती थी। वह दर्शक खींचने की मशीन था। कई बार तो यह भी होता था कि मंच पर परदा पड़ा होता और लहँगा-चोली पहनाकर नानक को चूनर का घूँघट करवाए एकाध बार ऐसे ही चक्कर लगवा दिया जाता था। उसे देखकर पहले-से आ जमे बच्चे अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते थे अपनी अम्मा-बुआ-जीजी को यह बताने कि ‘बैरी कजरा’ गाने वाली औरत स्टेज पर टहल रही है।
लेकिन नेमचंद उर्फ़ नेमा को यह सब अच्छा नहीं लगता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला के बीच नाच-गाना करने वाले टोटके उसे वाहियात और बेहूदे लगते थे। दिन में हम कभी उनके आसपास बैठे हों और कोई धार्मिक चर्चा न छिड़े, यह हो नहीं सकता था। एक दिन रामलीला की बात चली तो नेमा ने कहा, “कहाँ भगवान राम कौ त्यागमयी चरित्रा और कहाँ उनकी लीला कूँ बीच में रोककै दो टके के लौंडन्नै जनाने कपड़े पहनाकै नचानौ।” फिर रामलीला आयोजकों पर भुनभुनाते हुए बोले, “ऐसेई तौ सास के कन्नै वारे हैं और ऐसेई करवानै वारे हैं।”
“तो नेमा, तुम जाते ही क्यों हो उसे देखने?” हम में से एक ने टोका।
“मोय दिखाई देत्वै जो मैं देखवे कूँ जात हूँ?” उसे डाँटते-से स्वर में उन्होंने कहा; फिर बोले, “मैं तो जात हूँ रामकथा सुनवे कूँ।”
“चलो सुनने को ही सही...जाते क्यों हो ऐसी जगह जहाँ ओछी बातें सुननी पड़ें।” दूसरे ने कहा।
“साधू ऐसौ चाहिए जैसौ सूप सुभाय, सार सार कूँ गहि लए थोथौ देय उड़ाय……समझौ?” वह बोले, “मैं वहाँ जात हूँ—सार सार गहवे कूँ थोतौ गहवे कूँ नईं।”
सोने का हिरन
हमारे जानते तो नेमचंद जन्म से ही अंधे थे। उम्र के लिहाज से हमारे पिताजी की नहीं तो चाचा की उम्र के तो ज़रूर रहे होंगे। हालाँकि उनके भाई-भतीजे सब थे; लेकिन मन उनका अपने जीजा के घर में ही रमता था। बड़े भाई ने देखभाल के बहाने उनकी जमीन के कागज हथिया रखे थे। उसका कहना था कि ‘नेमा को दे दिए तो कोई चालाक आदमी अँगूठा लगवाकर जमीन को हड़प लेगा।’
“अजी हाँ, कैसें हड़प लेयगौ? मैं अंधौ जरूर हूँ, मूरख नाऊँ।” नेमा जहाँ-तहाँ कहते-फिरते थे। उनकी तथाकथित ‘बुद्धिमानी’ से बचने के उद्देश्य से बड़े भाई ने उनके हिस्से की ज़मीन को अपनी बताते हुए जिला कचहरी में उन पर मुकदमा ठोंक रखा था। केवल जीजा को पता था कि यह मुकदमा जमीन को बिकने से बचाने के लिए ही ठोंका गया है, बदनीयती से नहीं। नेमा के हिस्से की पैदावार को बेचकर बड़ा भाई सारी रकम जीजा को सौंप जाता था। वे उस रकम से ही नेमा के रहने, आने-जाने और मुकदमे की पैरवी का खर्चा उठाते थे। इस तरह पैतृक ज़मीन को अंधे भाई की संभावित नादानी से बचाने की खातिर बड़ा भाई गाँवभर की और नाते-रिश्तेदारों की नज़र में विलेन बना हुआ। इस रहस्य को या तो स्वयं वह जानता था या जीजा। उसके अपने बीवी-बच्चे या जीजी भी इसे नहीं जानती थी।
खुद के घर के बच्चों से लेकर गाँवभर के बच्चों तक में कोई भी उन्हें चाचा, ताऊ, बाबा, भैया, मामा नहीं कहता था। सब के बीच वे ‘नेमा’ नाम से जाने जाते थे। कुआँरे थे और अनपढ़ भी; लेकिन कबीर, रहीम, मीरा, दादू कौन-सा भक्त कवि था जिसकी कम से कम एक रचना उन्हें याद न हो। तुलसी तो उन्हें जैसे समूचे ही रटे पड़े थे—रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका सब-कुछ। इनके अलावा आल्हा-ऊदल, नल-दमयंती, सरवर-नीर, शिवजी का ब्याह, नरसी का भात...और भी कितनी ही लोकगाथाएँ उन्हें रटी पड़ी थीं। कैसे और कहाँ से रटी उन्होंने ये सब!!! हमें सोचकर ही ताज्जुब होता था। ‘राम’ को लेकर वे इतने संवेदनशील थे कि उनके बारे में हर तर्क उन्हें कुतर्क लगता था। एक बार हुआ यह कि पिछली रात छोटेलाल ने सीताहरण वाला भाग मंचित किया था और अगली दोपहर को हम नेमा के चारों ओर बैठे थे। चर्चा सोने के हिरन की छिड़ गई।
“नेमा, सीता के कहते ही राम सोने के हिरन के पीछे तीर-कमान लेकर क्यों भाग निकले? जोरू के गुलाम थे क्या? ” एक ने कहा।
“जोरू के गुलाम वारी या में का बात है गई?” उसकी बात से किंचित चिढ़कर नेमा ने कहा, “तेरे कहतेई जो तेरौ बाप तोकूँ कापी-पेंसिल ला देवै है तो का वो गुलाम ह्वै जावै है तेरौ?”
“पर, कॉपी-पेंसिल लाने में और जीव-हत्या के लिए जाने में तो बहुत अन्तर है ना।” उसने कहा।
“कोई अन्तर नाँय।” नेमा ने कहा, “घर में जब खावे कूँ दाने ना होवैं और उधार माँगकै बच्चन कूँ कापी-पेंसिल लानी परै है तो जीव-हत्या ही होवै है माँ-बाप की।”
“अच्छा चलो, मान ली तुम्हारी बात।” वह आगे बोला, “फर्ज़ करो कि हिरन मारीच न होकर सचमुच सोने का ही होता। तब उसे मारकर उसकी खाल कैसे लाते राम?”
“उतारकै लाते, और कैसे लाते?” नेमा ने उत्साहपूर्वक कहा।
“लेकिन मरे जानवर की खाल उतारने का काम तो उन दिनों चमार करते थे।” उसने तर्क पेश किया, “तो राम क्या चमार थे जो खुद खाल उतारकर लाते?”
उसकी यह दलील सुनकर नेमा की आस्था को तेज़ धक्का लगा। उनका चेहरा तमतमा उठा। गुस्सेभरी आवाज़ में बोले, “राम कूँ चमार बतावै है हरामखोर! ये लै... ” यों कहकर बैठे हुए नेमा ने बायें कंधे पर टिका रखी लाठी को दायें हाथ में उठाया और अपने सिर के चारों ओर गोल-गोल घुमाना शुरू कर दिया। फुर्ती के साथ उस लाठी की रेंज से बाहर हो जाने के हम अभ्यस्त थे, सो हो गये और इस तरह चोट खाने से बच गये। नेमा की अंध-आस्था से खिलवाड़ के ऐसे मौके अक्सर ही आते रहते थे। ‘राम’ के खिलाफ वे एक शब्द भी सुन नहीं सकते थे। खूँखार हो उठते थे; लेकिन उनका वह खूँखारपना स्थाई नहीं होता था। कुछ देर बाद सब-कुछ भूलकर वह सामान्य हो जाते थे और पहले की तरह ही बातें करने लगते थे।
गली रंडियों वाली
उसी साल क्वार माह वाले नवरात्रों की बात है। नेमचंद मुँह-अंधेरे ही नहा-धोकर तीन-चार कोस दूर दुर्गा देवी के मंदिर में पूजा करने को जाते थे। वही क्या, पूरा शहर उसी मंदिर को जाता था उन दिनों। हम भी जाते थे और अक्सर नेमा के आगे-पीछे ही रहते थे। एक दिन हम जल्दी लौट आए और नेमा पीछे अकेले रह गये। हो सकता है कि हताश-निराश उन्होंने एक-दो आवाज़ें लगाकर हमें पुकारा भी हो। खैर। वे अकेले ही लौट पड़े। अब, आगे की कहानी अपने जीजा से उनकी खुद की जुबानी सुनो:
“जीजा, चलतौ-चलतौ चैक बजार में सिकारपुरिया की दुकान तक तौ मैं ठीक-ठाक आ गयौ।”
“तुझे कैसे पता पड़ी कि ये शिकारपुरिया की दुकान है?” जीजा ने पूछा।
“आँखई तौ खराब हैं जीजा, नाक-कान थोरेई खराब है।” नेमा ने उलाहने के साथ कहा, “देसी घी की खसबू और जरेबी सिकनै की छनन-छनन अवाज ते जान गयौ कै ये सिकारपुरिया हरवाई की दुकान है।”
“फिर?”
“फिर काई बदमास नै मज़ाक कर डारौ।”
“क्या?”
“इधर नईं सूरदास इधर-यों कहकै मेरी लठिया दूसरी लंग कूँ टिका दीन्ही। मैं वाई लंग कूँ आगै बढ़ गयौ।”
“किधर को?”
“बताऊँ हूँ... ” नेमा ने कहा, “पैरन के नीचै सिमंट की सड़क की जगै ईंटन कौ खरंजा आन लगौ तौ मेरो सिर चकरायौ।”
“गली में घुस गए क्या?” जीजा ने चुटकी ली।
“घुस का जान-बूझकै गए...वा लम्पट नै भटका दए सो घुस गए... ” नेमा चिढ़कर बोले।
“चलो, जैसे भी घुसे, घुस तो गये।” जीजा बोले, “हम तो आज तक तरस रहे हैं...हिम्मत ही नहीं होती है।”
“फिर वोई बात!” नेमा गुसियाकर बोले, “तुमैं हमाई सौं है जीजा, ओछौ मज़ाक मती करौ।”
“अच्छा नहीं करेंगे।” जीजा ने कहा, “आगे सुनाओ।”
“घबराकै मैंनै लठिया सै दाएँ-बाएँ टोहकै देखी। लठिया दाएँ भी सिड्डिन सै टकराई और बाएँ भी। इत्ती पतरी गरी! छिद्दा की बात याद आन लगी।”
“क्या?”
“वो कहवै हौ कै जब भी तारीख पै सहर कूँ आवै है, वो पतरी गरी में हैकै जरूर जावै है।”
“क्यों?”
“अब जानबूझ कै जे सब तुम मोते मती पूछो।”
“अच्छा, फिर तेरे साथ क्या हुआ?” जीजा ने नेमा से उसके बारे में पूछा।
“मोए ऐसौ लगौ कै आसपास लुगाई हँस रई हैं। पौडर-सौडर की खसबू भी आन लगी। मैं एकदम सै घबरा गौ। मोए पसीनौ आन लगौ।”
“क्यों?” जीजा ने जानबूझकर सवाल किया।
“चौं का?” नेमा चहके, “मैं और रंडिन वारी गरी में! सो भी नौरातिन में!! कछू रार है जाती तौ कलंक ना लग जातौ जिन्दगीभर कूँ।”
“फिर कैसे सूखा पसीना?”
“मैंने हिम्मत करी और लुगाइन की अवाज की तरफ बोलौ—माफ करना बहन जी... इतनी सुनतेई एक बोली—चुप बे अंधे की औलाद, बहन जी कहियो अपनी लुगाई को। ऐसी गंदी जबान सुनकै जीजा, मेरे तो होसई उड़ गए। फिर भी हिम्मत करकै बोलौ—हम रस्ता भटक कै या गली में आ गए हैं बह...ऽ....। बड़ी मुस्किल सै वायै ‘बहनजी’ कहवे ते रुकौ मैं। फिर बोलौ—बाहर कौ रुख करवा दो मेहरबानी करकै। ये सुनकै काई दूसरी नै अवाज लगाई—कोई है? लात मारकर गली से बाहर निकालो इस भड़वे को। सुबह-सुबह चला आया मनहूस शक्ल लेकर बोहनी खराब करने को। मैं डर गयौ। मोय तौ पहली बार पतौ चली जीजा, कै ‘बहनजी’ भी गारी होवै है। मैनैं मनई मन गुहार लगाई—हे दुर्गा माई! लाज रखौ। ह्याँ तौ बचान वारौ बी कोई नाँय। तबई एक छोरा नै परगट है कै मेरी लठिया पकरी और बोलौ—आप इधर आओ बाबा जी। वा भले आदमी नै मैं वा नरक सै बाहर निकार दीन्हौ। भगवान भलौ करै वाकौ।”
“और जो वो वही लड़का हो जिसने तुम्हारी लाठिया गली की ओर मोड़ दी थी, तब?” जीजा ने चुसकी ली।
“तबऊ देवी माँ वाकौ कल्यान करै।” नेमा ने कहा, “जोऊ करौ होय, बचायौ भी तो वाई नै। मैं तौ जानूँ कै वाय देवी मैया नैई गुहार सुनकै मेरी रच्छा कूँ भेजौ हौ।”
हुई वर्षा अमृत की
बहुत बड़ा आँगन था। घर के सभी लोग अपने-अपने कामों में लगे रहते थे। सुबह-सुबह तो किसी को कुछ चाहिए होता था और किसी को कुछ। भारी चिल्ल-पौं रहती थी। सो, उस वक्त नेमा घर पर नहीं रहते थे। अल-सुबह ही नहा-धोकर निकल आते थे बाबा राज राजेश्वर महाराज के मंदिर की ओर। घंटियों और घडि़यालों की आवाज़ उन्हें सुख देती थी। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, पिछवाड़े ही था घर के। हालाँकि लाठी उनके हाथ में रहती थी; लेकिन चलते वे उसका सहारा लिए बिना ही थे। चाल! दांडी-यात्रा पर निकले महात्मा गाँधी की चाल को भी मात देने वाली, ग़ज़ब की तेज़। रास्ते में पड़े गोबर के चोथ, ईंट-कंकड़ की बात छोड़ दें तो सजीव पात्रा खुद ही उनके रास्ते से हट जाते थे, कुत्ते भी। ईश्वर ने उन्हें आँखें दी होती तो निश्चय ही वे इतना तेज़ नहीं चल सकते थे।
मंदिर का प्रांगण काफी विस्तार लिए हुए था। वहाँ पहुँचकर नेमचंद एक खास दीवार में बने आले तक जाते थे। उसमें कुछ टटोलते थे; और उसे खाली पाकर पुकारते, “अभी सिर्राम नईं आए का?”
“आ गया हूँ महाराज!” पत्थर की सिल पर चन्दन घिस रहे लाला श्रीराम उनकी पुकार सुनकर बोलते थे, “घिस चुका। लाता हूँ अभी।”
लाला श्रीराम नादीद नहीं थे, लेकिन घर से वे भी सुबह-सुबह ही निकल भागते थे। पहले, मुँह-अँधेरे ही, वे दिशा-मैदान के लिए घर से निकलते थे। घूम-घाम, शौच, हल्का-फुल्का व्यायाम, दातुन और कुछ लोगों से दुआ-सलाम तक का काम वहाँ हो जाता था। घर आकर नहाते थे; और बस्ता उठाकर सीधे मंदिर को चले आते थे। बस्ता कुछ खास नहीं, बड़े आकार का रामचरितमानस, उसे टिकाने के लिए लकड़ी का रहल और सफेद चन्दन की एक बट्टी लाल कपड़े में लपेटकर रखी होती थी। मंदिर में एक कोना जैसे उनके लिए निर्धारित था। यों तो आसन वहाँ बिछा ही रहता था; फिर भी, किसी दिन अगर नहीं रहता तो इधर-उधर से ढूँढकर वे कुश का आसन लाते और कोने में बिछा देते थे। बस्ते को दीवार में बने आले में रखकर उसमें से चन्दन की बट्टी निकालते थे। गंगाजल मिले जल से भरा एक लोटा वे घर से लेकर चलते थे। मंदिर में हालाँकि कुआँ भी था, हैंडपंप भी और वाटर टैप भी; लेकिन भोले बाबा को स्नान कराने के लिए जिस जल पर उन्हें विश्वास था, वह घर से लाया हुआ गंगाजल मिला जल ही था।
बलराम अग्रवाल
जन्म : 26 नवंबर, 1952 को उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर मेंशिक्षा : पीएच॰ डी॰ (हिन्दी), अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
पुस्तकें :
कथा-साहित्य
सरसों के फूल (1994),
ज़ुबैदा (2004),
चन्ना चरनदास (2004),
खुले पंजों वाली चील (2015),
पीले पंखों वाली तितलियाँ (2015)
बालसाहित्य
दूसरा भीम (1997),
ग्यारह अभिनेय बाल एकांकी (2012),
अकबर के नौ रत्न (2015),
सचित्र वाल्मीकि रामायण (2015),
भारत रत्न विजेता (2015)
समग्र अध्ययन
उत्तराखण्ड (2011),
खलील जिब्रान(2012)
अनुवाद व पुनर्लेखन :
(अंग्रेजी से) अण्डमान व निकोबार की लोककथाएँ (2000); अनेक विदेशी कहानियाँ व लघुकथाएँ; लॉर्ड आर्थर सेविले’ज़ क्राइम एंड अदर स्टोरीज़ (ऑस्कर वाइल्ड)। (संस्कृत से) सम्पूर्ण वाल्मीकि रामायण (2014)
संपादन : मलयालम की चर्चित लघुकथाएँ (1997), तेलुगु की मानक लघुकथाएँ (2010), समकालीन लघुकथा और प्रेमचंद (आलोचना:2012), राष्ट्रप्रेम के गीत:जय हो! (2012), लघुकथा:पड़ाव और पड़ताल खण्ड-2 (2014); कुछ वरिष्ठ कथाकारों की चर्चित कहानियों के 25 संकलन।
संपर्क : एम-70, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032
मोबाइल : +918826499115
ई-मेल : 2611ableram@gmail.com
चन्दन की बट्टी को पत्थर की जिस सिल पर घिसना होता, पहले वे उसे मंदिर के कुएँ वाले पानी से अच्छी तरह धोते थे। फिर चबूतरे वाले पीपल से चौड़े-चौड़े तीन पत्ते तोड़कर लाते और चन्दन घिसना शुरू करते। तीन पत्ताभर चन्दन घिस जाने के बाद वे उठते और राजराजेश्वर महाराज का जलाभिषेक करते, एक पत्ताभर चन्दन से उनका शृंगार करते; दूसरे पत्ताभर चन्दन को अन्य श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के एक निश्चित आले में रखते तथा तीसरे को लेकर मंदिर की शेष मूर्तियों का अभिनन्दन करते।
होता अक्सर यह था कि नेमचंद को चन्दन आले में रखा मिल जाता था; लेकिन कभी-कभी नहीं भी मिलता था। पीपल का पत्ता होता ही कितना भारी है। हवा जरा तेज़ हुई नहीं कि चन्दन से भरा होने के बावजूद पैर उखड़ जाते थे बेचारे के। आ पड़ता था ज़मीन पर। एक बार तो हुआ यह कि पत्ता ज़मीन पर पड़ा था और नेमचंद का पैर उस पर पड़ गया।
“राम-राम राम-राम, ” गीले चन्दन का आभास पाते ही हड़बड़ाहट में उनके मुँह से निकला, “लाला सिर्राम हैं, कै चले गए!”
“यहीं हूँ महाराज! बाबा राजराजेश्वर को रामचरित सुना रहा हूँ, आ जाओ।” कोने में बैठकर मानस का पाठ कर रहे लाला जी बोले।
“गजब है गयौ भाई, ” नेमचंद बोले, “तुम्हारे चन्दन पै पैर पड़ गयौ आज।”
सामने बैठा रखे भोले बाबा से मन ही मन क्षमा माँगकर लाला जी उठे और बाहर आकर देखा। बोले, “चन्दन भी अपनी सही जगह ढूँढ़ ही लेता है महाराज। आज आपके चरणों का अभिषेक हो गया।”
“चौं मोए पाप कौ भागीदार बना रए हौ लाला।” नेमचंद ने कहा, “पिछले करमन की तौ अब भोग रह्यो हूँ। अगले जनम में भी याई गत कूँ भोगने की जुगत चैं बना रए हौ।”
“अभी आप यहीं खड़े रहो, मैं दूसरे पत्ते पर रखा हुआ चन्दन लाता हूँ।” यों कहकर लाला जी गये और हैंडपंप चलाकर लोटे को भर लाए। उस जल से उन्होंने नेमचंद के पाँव यों पखारे कि नेमचंद कुछ समझ ही न पाएँ। उन्हें पैर धोते पाकर वे बस इतना ही बोले, “अरे सिर्राम, इनैं तौ मैं खुदई धो लेतौ नर पै जाकै। तुम मोए चन्दन ला दो, बस।”
उनके यों कहते ही लाला जी ने चन्दनभरा दूसरा पत्ता उनके आगे कर दिया; बोले, “ये लो।”
थोड़ा टटोलकर अनामिका के पोर से चन्दन का टीका नेमचंद ने अपने माथे पर लगाया और बोले, “सिर्राम, तुम रोज भोले बाबा कूँ रामायन सुनाओ हो, आज मैं तुमैं कछु सुनाउँगौ। सुनौगे?”
“यह तो बड़े सौभाग्य की बात होगी महाराज, क्यों नहीं?” लाला जी तुरन्त बोले और नेमचंद को साथ ले अपने आसन की ओर बढ़ आए। उनको उन्होंने अपने आसन पर बैठाया और खुद उनके सामने बैठे। नेमचंद मंदिर के चप्पे-चप्पे से परिचित थे। वे समझ तो गए कि लाला जी ने उन्हें अपने आसन ला विराजा है; लेकिन कहा कुछ नहीं। कुछ देर वे मौन बैठे रहे; फिर पूछा, “बाधा तौ नाँय पड़ैगी काई कूँ?”
“नहीं महाराज, रास्ते से मैं काफी अलग बैठा हूँ।” लाला जी ने कहा।
“सो बात नईं, ” नेमचंद बोले, “मेरौ मतलब है कै ऊँचे सुर में गाउँगौ तो काई और की पूजा में तौ बाधा नाँय पड़ैगी?”
“रस की धारा कभी बाधा थोड़े ही बनती है महाराज, ” लाला जी ने कहा, “आपके मुँह से भजन सुनना तो सौभाग्य की बात होगी सब के लिए।”
“ठीक है, ” वे बोले, “तौ सुनौ... ” यों कहकर उन्होंने अपने सलूके की जेब में हाथ डाला।
आठ-दस इंच लंबी पतली-सी कोई टहनी, लकड़ी या सरकंडे का टुकड़ा वे हमेशा सलूके की जेब में रखते थे। उसे निकालकर उन्होंने दायें हाथ की बीच वाली तीन उँगलियों में फँसाया और डुगडुगी की तरह पंजे को हिलाने लगे। कुछ ही देर बाद, बिना पुतलियों वाली उनकी आँखें भौंहों की ओर उठने लगीं और पलकें नीचे की ओर झपकने लगीं। यह मस्तिष्क के एकाग्र होते जाने की मुद्रा थी। पाँच-सात मिनट बाद, एक खास क्रम में उनका सिर भी झूमने-सा लगा; जैसे कि भीतर ही भीतर वो संगीत की फुहारों में भींगने और नाचने लगे हों। लाला श्रीराम श्रद्धापूर्वक उनकी ओर देखते बैठे रहे। कुछेक मिनट और बीत जाने के बाद नेमचंद के कंठ से रस की धारा बहनी शुरू हुई:
राम राम रमु, राम राम रटु, राम राम जपु जीहा।
रामनाम-नवनेह-मेहको, मन हठि होहि पपीहा।।
सीधे हाथ की उँगलियों में फँसी डंडी की डुगडुगी सुर और ताल के अनुसार तेज़ और धीमी हो जाती थी। बायाँ हाथ लगातार उनके घुटने पर थाप लगा रहा था। इन दोनों पंक्तियों को उन्होंने सुर साधने की दृष्टि से कई बार दोहराया; जैसे कि सुर को साधे बिना पद के आगे का हिस्सा वे गा न पा रहे हों। पूजा-अर्चना करके मंदिर के भीतर से निकलने वाले लोगों में अधिकतर उन्हें पहचानते थे। कई ने अनेक बार उनका गायन सुन रखा था। उनमें से कुछ बाबा राजराजेश्वर को मत्था टेककर उनके आसपास जमीन पर ही बैठ गये। चार-छह बार दोहराने के बाद उनका सुर सध गया। एक बार पुनः पहले वाली लाइनों को दोहराने के बाद उन्होंने पद की अगली लाइनें पकड़ीं; गोया कि पद को शृंखलाबद्ध किया। फिर समापन भी शुरू की लाइन गाते हुए ही किया:
राम राम रमु, राम राम रटु, राम राम जपु जीहा।
राम राम रमु, राम राम रटु, राम राम जपु जीहा।
पद को पूरा गाकर वे चुप बैठ गये, जैसे कि राम-नाम की सरिता में तलहटी पर जा बैठे हों; जल-समाधि ले ली हो। लाला श्रीराम और आसपास बैठे बाकी सब लोग आनन्द-विभोर हो उनकी ओर ताकते हुए शान्त बैठे रहे। कुछ पल बाद स्वयं नेमचंद ही ऊपर आए। बोले, “कैसी रही सिर्राम?“
“अद्भुत! आनन्द आ गया महाराज।” लाला जी के मुँह से निकला।
“ऐसैई कभी-कभी तुमहू अपने भीतर नहाया करौ।” नेमचंद ने कहा।
“मेरा गला इतना मधुर कहाँ है महाराज।” लाला जी ने कहा।
“भीतर नहावे के ताईं करवौ-मीठौ गलौ थोरेई देखौ जात्वै। वाके ताईं तौ मन में भाव हौनौ चइयै, बस।” नेमचंद ने कहा, “एक बात सुनौ सिर्राम, जो आदमी खुद कूँ खुस ना रख सकै वो दूसरन्नै कैसै खुस रख सकै है, सोचै।”
“सो तो है।” लाला जी दबे-स्वर में बोले जैसे कि वे नेमचंद की बात का विरोध करने से बच रहे हों।
“जो पद अभी-अभी मैंने गायौ, वो विनय-पत्रिका कौ है, उनई बाबा तुलसीदास कौ लिखौ भयौ जिनकी लिखी रामायन तुम भोरे बाबान्नै सुनाऔ हौ रोज।” नेमचंद बोले, “अभी मेरौ मन भरौ नाय। एक पद और गाउँगौ। तुमैं देर हो रई होवै तो उठकै चले जइयो, मोए टोकियो मती।”
“कैसी बात करते हैं महाराज, ” लाला जी ने हँसते हुए कहा, “कितने सौभाग्य से तो गाने की इच्छा आप के मन में आज खुद ब खुद जागी है! उसे भी मैं बीच में छोड़कर उठ जाऊँ!! यह कैसे हो सकता है। पूरा का पूरा सुनूँगा।”
इधर लाला जी अपनी बात कहते रहे, उधर नेमचंद ने दूसरा पद गाने के लिए सुर को साधना शुरू कर दिया। दायें हाथ की डुगडुगी तेज़ी से हिलने लगी। घुटने पर बायीं हथेली की थाप पुनः पड़नी शुरू हो गयी। नेमचंद ने गाना शुरू किया:
राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे।
घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे।।
राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे।
मंदिर में घंटियाँ भी बज रही थीं और घडि़याल भी; लेकिन यहाँ एकदम सन्नाटा था। नेमचंद की वाणी का रस आसपास बैठे एक-एक व्यक्ति को भिगो रहा था। सब विभोर थे। कब पद खत्म हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। सब यही समझकर चुप बैठे रहे कि नेमचंद ने अर्द्ध-विराम लिया है।
“सिर्राम!” चुप्पी के घटाटोप को आखिर नेमचंद की आवाज़ ने ही चीरा।
“जी महाराज।”
“तुमारौ पाठ रुकवाकै आज गलत तौ ना कर दियौ कछू? छोह तौ नाँय मन में?”
“आप क्यों मुझे शर्मिन्दा कर रहे हैं महाराज। बाबा राजराजेश्वर की मर्जी आज आपके मुँह से पद सुनने की थी सो उन्होंने सुन लिए।“ लाला जी ने कहा, “उनके बहाने हमारे भी कानों में राम-नाम पड़ गया, हमारा भी जीवन सफल हो गया।”
“बारिस में खूब भीग लियौ मैं आज... तिरप्त है लियौ।”
“हम भी सूरदास जी।” बैठे लोगों में से कोई बोला और उठकर चल दिया। नेमचंद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, न उधर ध्यान ही दिया; लेकिन लाला जी को उसका उन्हें ‘सूरदास’ कहना बहुत अखरा। उन्होंने कठोर नज़रों से उसकी ओर देखा लेकिन उठकर खड़ा हो जाने के बाद उसने किसी की ओर कतई ध्यान नहीं दिया और चला गया।
“एक बात कहूँ सिर्राम, तुम में और मो में येई फरक है कै तुम सुननै और सुनानै में यकीन करौ हौ... ” नेमचंद आगे बोले, “मैं सुनाऊँ काउऐ नाउँ। जब भी मन करै है, खुदई गाऊँ हूँ और खुदई कूँ सुनाऊँ हूँ। मैं खुदई बादर होत हूँ, खुदई बारिस और खुदई भीजनहार।”
नेमचंद का गायन खत्म होने के बाद ये दार्शनिक बातें शुरू हो गई थीं। आ बैठे किसी भी व्यक्ति की रुचि इन बातों में नहीं थी इसलिए एक-एक कर सभी उठकर जाने लगे। यों भी सवेरे का समय था। किसी को दफ़्तर जाने की चिंता थी तो किसी को जाकर दुकान खोलने की। जब सभी जा चुके और लाला जी अकेले बैठे रह गये तब नेमचंद ने कहा, “मैं जानूँ हूँ कै तुम औरन की ताईं कछु माँगो ना हौ भगवान सै। निस्वार्थ भाव सै रामायन सुनाऔ हौ विनकूँ। पर मेरे कहे ते, एक बार खुदई कूँ सुना कै देखौ।”
“खुद को कैसे सुनाऊँ?” लाला जी ने पूछा।
“वैसैई जैसै उनैं सामनै बैठाकै सुनाऔ हौ।” नेमचंद बोले, “जामें मुस्किल का है? अरे, जायै सामने बैठाकै सुनाऔ हौ वायै अपने भीतर बैठाकै सुनान लगौ, बस। वानै एक बार भीतर बैठकै सुन लई तौ समझ लो कै वायै बाहर बैठाकै सुनावे में फिर आनन्द ना अवैगौ कबहूँ।”
नेमचंद की बातें लाला जी को अपनी समझ की सीमा से परे लग रही थीं, सो उन्हें सुनकर वे हाँ-हूँ तो कर रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे।
“एक बात और कहूँ सिर्राम... ”
“जी महाराज।”
“तुमनै चन्दन धोनै के बहाने जो आज पाँव पखारे मेरे, सो मैं वाके लायक कतई ना हूँ। अंधौ बाम्हन हूँ, पुरखन के लिखे दो-चार पद गा लेत हूँ, बस। कोई और खूबी मो में नाँय।”
लाला जी कुछ न बोले। बैठे रहे चुपचाप।
“अब तुम अपनौ पाठ पूरौ करौ। मैं कहीं और बैठ जात हूँ जाकै।” नेमचंद बोले।
“आप यहीं बैठे रहो महाराज।” लाला जी बोले, “आज का पाठ मेरा पूरा हो चुका। मैं अब चलूँगा।” यों कहकर वे अपना बस्ता सम्हालने लगे।
नेमचंद ने डुगडुगी हिलानी शुरू कर दी। सुरों ने उनके भीतर बादल का रूप लेना शुरू कर दिया और बेआवाज़ वे बरसने भी लगे। खुद ही पैदा किए रस की बारिश में नेमचंद नहाने भी लगे हैं, कोई नहीं जानता था।
००००००००००००००००












0 टिप्पणियाँ