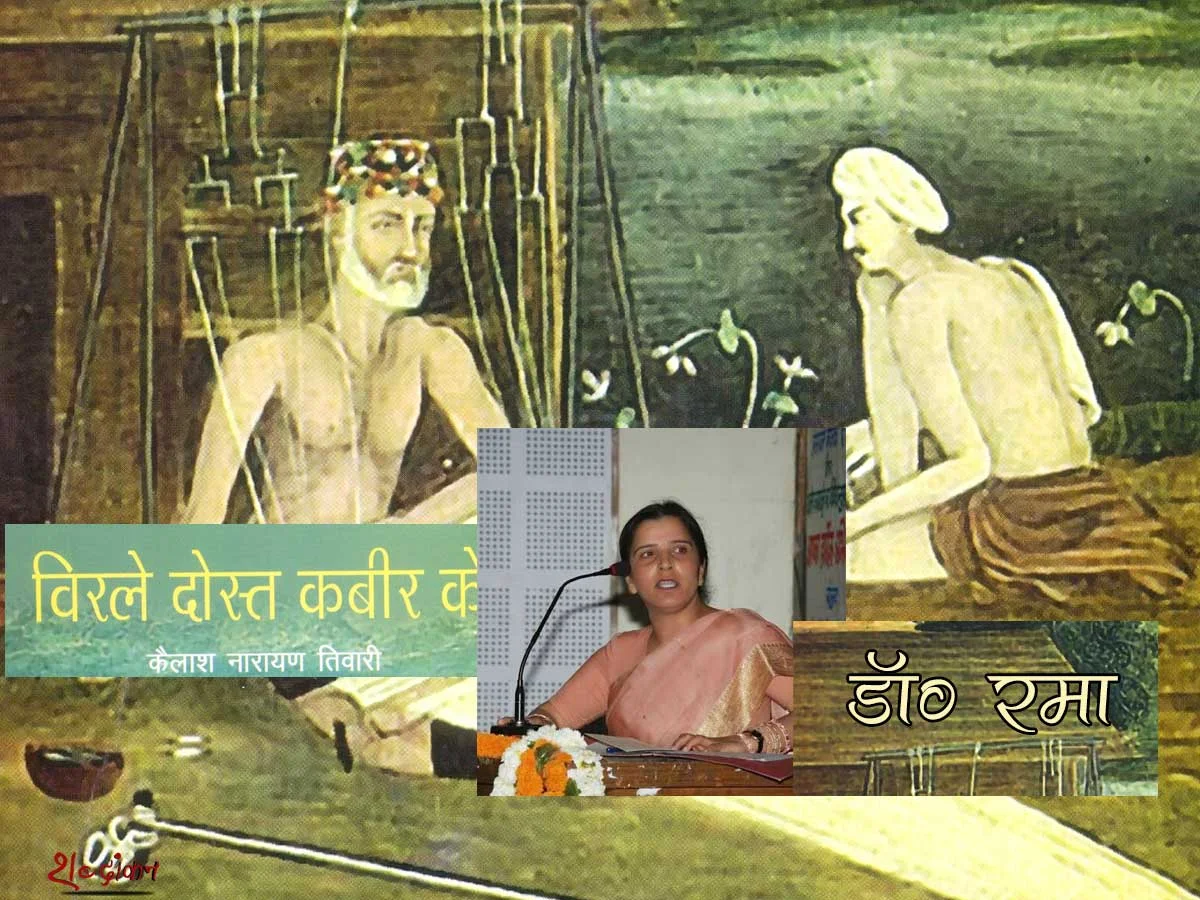
नए कबीर की खोज में
- डॉ॰ रमा
description
सच कहूँ तो यह उपन्यास मेरे पास समीक्षा के उद्देश्य से आया ही नहीं था। किसी ने यह कहकर कर पकड़ा दिया था कि– “पढ़िएगा, नए कबीर दिखेंगे”। पढ़ना तो क्या व्यस्तता में बहुत दिनों तक पुस्तक देख भी नहीं पायी। इधर कुछ दिन पहले जब कबीर केन्द्रित प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक के लिए लेख मांगा गया तो अचानक इस पुस्तक की याद आयी। पढ़ना शुरू किया तो रख नहीं सकी। सच में इस उपन्यास को पढ़ते हुए मैं नए कबीर से परिचित हो रही थी। ऐसे कबीर से जिनकी पीड़ा किसी साधारण मनुष्य की सी थी। पहली बार मैं ऐसे कबीर को पढ़ रही थी जिसके नेत्र भीगे हुए हैं। अभी तक हिन्दी साहित्य में कबीर की छवि ऐसे नायक के रूप में व्यक्त की जाती रही है जो हाशिये के समाज के लिए आजीवन अपनी कविताओं से जूझते रहे। कबीर का महाकाव्यात्मक उदात्त चरित्र वर्षों से हमारी चेतना से ऐसे बैठ गया है कि साधारण व्यक्ति के साँचे में उन्हें ढालने का साहस ही नहीं कर पाते। पर रचनाकार हमेशा बड़ा होता है वह अपनी कल्पना से चरित्र के भीतर तक घुसने की छूट ले लेता है। कैलाश नारायण तिवारी ऐसे ही रचनाकार हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए लगातार महसूस होता है कि उन्होने का कबीर अध्ययन बहुत बारीकी और गंभीरता से किया है। कबीर के व्यक्तित्व को समझाने के उन्होने जिन कविताओं का चुनाव किया है वह कई दृष्टियों महत्वपूर्ण है। दरअसल कबीर का अधिकतर मूल्यांकन उनके ‘दोहों’ में निहित संवेदना के आधार पर ही किया गया जबकि उनके गेय छंदों में उनका विचार गहराई से उभरकर सामने आता है। एक तरह से देखें तो कबीर का सम्पूर्ण काव्य तत्कालीन भारतीय समाज की राजनीति, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और मनुष्यता में आ गयी विकृति की औषधि है। कबीर उसके वैध हैं। उनकी कविता मनुष्य और मनुष्यता के बीच सामंजस्य बैठाने वाले सूत्रों का शोध करती है और कबीर शोधार्थी है। अभी तक हमारा जिस कबीर से परिचय हुआ है वह एक महान और विख्यात कवि हैं, समाज सुधारक हैं, भाषा सिद्ध काव्य चिंतक हैं परंतु “विरले दोस्त कबीर के” में वह मात्र एक साधारण मनुष्य हैं। एक ऐसे व्यक्ति से साक्षात्कार हुआ जो अपने समाज की बिडंबनाओं को देखकर अंदर तक दुखी है। कबीर का सम्पूर्ण जीवन मनुष्यता की खोज में बीता। वह आजीवन समाज को यही समझाते रहे कि ईश्वर की तलाश अपने अंदर करो बाहर उसका अस्तित्व बहुत झीना है उसे देखने के लिए कई बाधाओं से पर होना जरूरी है पर लोगों ने नहीं समझा। आज जो धार्मिक व्यापार का इतना व्यापक बाज़ार खड़ा हुआ है यह उसी का फल है।
सभी जानते हैं कबीर का जीवन का पहला अध्याय ही ‘गुरु’ की खोज से आरंभ होता है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है। आलोचकों से रामानन्द और कबीर के संबंध को बस यह कहकर ताल दिया है कि, काशी के मंदिर की किसी सीढ़ी पर लेते हुये कबीर पर रामानन्द का पैर पड़ जाता है और उनके मुँह से ‘राम’ शब्द का उच्चारण हो जाता है जिसे कभी मंत्र के रूप में स्वीकार कर लेते है। परंतु उपन्यासकर कुछ तथ्यों की तरह भी उन्मुख होता है । रामानन्द और कबीर के संबंध के कुछ और भी सूत्र खोलता है। वह लिखते हैं -“इतिहास और साहित्य इस बात पर चुप है कि कबीरदास गुरु रामानन्द के कितने करीब थे ? गुरु कि संगत में आने के बाद अपनी जिज्ञासाओं का या अपने प्रश्नों का निवारण वे किस सीमा तक कर पाये? दरअसल इस संबंध में कुछ थोड़े से सूत्र कबीर के पदों और दोहों में मिलते हैं। कबीर ने अनेक पदों और दोहों में गुरु कि महिमा का बखान किया है।” इस तरह देखें तो कई नई बात पता चलती है, जिसे रचनाकार ने बहुत ही सहजता से प्रस्तुत कर दिया है। इस उपन्यास में कई स्थानों पर कबीर की गुरु ढूँढने की व्याकुलता और छटपटाहट को रेखांकित किया है साथ ही कई जगहों पर उनका संवाद भी हुआ है जिसमें रामनन्द कबीर के ‘आंखिन देखी’ ज्ञान से विस्मित भी होते हैं और प्रसन्न भी। हिन्दी आलोचकों ने कबीर और रामानन्द के इस संबंध में कम ही चर्चा की है।
उपन्यासकार ने कबीर के महत्व को समझने के लिए उनका बकायदा अध्ययन किया है। हालाकि यह पुस्तक कबीर के ऊपर आलोचना नहीं है बल्कि उपन्यास है जिसमें रचनकर ने कई स्थानों पर कल्पना का सहारा लिया बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि कल्पना के माध्यम से कबीर का यथार्थ रच दिया है। वैसे भी यथार्थ के करीब पहुँचने के लिए कल्पना का सहारा लिया ही जाता है। लेकिन उपन्यास निरा-कल्पना भी नहीं है। रचनाकार ने जो तर्क दिया है और बात को जिस सलीके से रखा है वह कहीं भी भ्रमित नहीं करता है। कबीर के प्रादुर्भाव के संबंध में उन्होने एक स्थान पर लिखा है- “मध्यकालीन रूढ़िग्रस्त भारतीय समाज में सचमुच एक विचित्र। इतिहास ने समाज को एक ऐसा नायक, ऐसा योगी दे, एक ऐसा सत्यान्वेषी कवि दे दिया था जिसके पीछे चलने के लिए ढेर सारे लोग विवश हो गए थे। वह विवशता आगे चलकर इतिहास कि जरूरत भी बन गयी और क्षति-पूर्ति का साधन भी।” यह सच भी है। कबीर पूरी भक्ति कविता के ऐसे कबीर के रूप में चिन्हित हैं जिनकी काव्य चेतना जितनी प्रखर है स्वभाव भी उतना ही तेजस्वी है। वह बिसंगतियों पर कटाक्ष ही नहीं करते बल्कि उससे भिड़ भी जाते हैं। उनकी कविया की सबसे बड़ी विशेषता उसका विषय बद्ध न होना है साथ ही किसी एक भाषा और बोली बंधकर नहीं लिखना है। उन्होने अपनी कविता के लिए किसी एक विषय को नहीं चुना न किसी एक भाषा का चुनाव किया। हिन्दी के आलोचकों ने इसे एक कमी के रूप में भी देखने की कोशिश की पर देखना यह भी है की कबीर की कविता का फ़लक इसीलिए अन्य कवियों से बड़ा है। उनकी भाषा और विषय वस्तु नैतिक शिक्षा की तरह हैं जिसे अनपढ़ भी आसानी से समझ जाए और बौद्धिक भी चकरा जाए।
यह उपन्यास कई दृष्टियों से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हम पहली बार कबीर के चरित्र के अंदर तक प्रवेश कर पाते हैं। इतना ही नहीं कबीर के अन्तर्मन में छुपे उन रहस्यों से परिचित होते हैं जो कभी उनकी कविता में आसानी से नहीं देख पते हैं। अपने गहन अध्ययन से रचनाकार वहाँ तक पहुँचने में सफल हो जाता है। इसी संदर्भ में देखें तो कई स्थानों पर उपन्यासकार ने कबीर के प्रकृतिप्रेमी होने की चर्चा की है। एक स्थान पर उन्होने लिखा है कि- “कबीर प्राकृतिक उपदानों को जीवन की अमूल्य निधि मानते हैं क्योंकि प्रकृति से उनका निकट का संबंध था। पूरी-पूरी रात वह प्रकृति की गोद में बैठे बिता देते थे उस दिन भी बस एक ही बात लगातार सोचते रहे- ‘यह प्रकृति भी कितनी ममतामयी हैं। कितनी आनंददायिनी है। समान भाव से अपना सर्वस्व लुटा देती है; मनुष्य के ऊपर।” बहुत संभव है कि रचनाकर ने यहाँ पर भी कल्पना का सहारा लिया हो परंतु प्रकृति के प्रति कबीर के इस प्रेम-वर्णन में कहीं कोई अतिश्योक्ति नहीं झलकती है।
कबीर कि कविताओं में समाज ने अपनी पीड़ा तो ढूंढ ली गयी पर स्वयं उनका दुख: नहीं खोज पाया उपन्यासकार ने इस दिशा की तरफ भी ध्यान दिया है। उन्होने यह स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण भारतीय समाज को मानसिक बल देने वाली कबीर कि कविताओं में स्वयं उनके भी हृदय के उद्गार छुए हुए हैं। कबीर अपनी कविता में लगातार अपना दुख: व्यक्त कर रहे थे, बस उसे वह आम जनता से जोड़ देते थे जिससे लोग उसे सामाजिक मान लिया करते थे। रचनाकर ने लिखा है- “दुर्भाग्य से कम ही लोग जानते हैं कि कबीर का जीवन-संघर्ष उनकी कविता में निहित है जो हमेशा हमारी चेतना में गूँजती है। उनकी जीवन-यात्रा का सबूत स्वयं उनकी साखी, सबद रमैनी और पद हैं।”
सामयिक विमर्शों के केंद्र कबीर सबसे अधिक छाए रहे। चाहे वह दलित विमर्श हो या स्त्री विमर्श कबीर हर जगह याद किए जाते हैं। हिन्दी आलोचना में कबीर कि छवि स्त्री विरोधी ही व्यक्त कि गयी है। जहां वह नारी को बार-बार ‘माया महा ठगिनी’ कहते हैं। पर यह अंधूरा सच है। कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि उन्होने स्त्री का विरोध भी स्त्री कि रक्षा के लिए किया। उस समय स्त्री का मात्र भोग कि वस्तु समझा जाता था। चूंकि कबीर की वाणी का प्रभाव लाखों लोगों पर था इसलिए ‘माया’ कहते ही वह पुरुषों द्वारा भोग के दृष्टिकोण से मुक्त भी हो गयी होंगी। हलाकी यह विवाद का विषय हो सकता है परंतु इस उपन्यास को पढ़ते हुये यह महसूस होता है कि कबीर अपने माँ के बहुत करीब थे। यह पूरा उपन्यास ही कबीर से अपनी माँ नीमा से संवाद है। वह अपनी पत्नी लोई का भी आभार व्यक्त करते हैं। अपनी माँ और पत्नी का हद से ज्यादा आदर करने वाला व्यक्ति स्त्री विरोधी कैसे हो सकता है? इस प्रश्नों का जबाब बहुत तार्किकता से इस उपन्यास में मिल जाता है। रचनाकार ने कई स्थान पर इसका उदाहरण भी दिया है। यथा- “कबीर के जीवन में उन्हें सर्वाधिक प्रभावित करने वाली खास तौर पर तीन औरतें थीं। पहली औरत ‘माया’ थी जिसे जगत माता भी कह सकते हैं। दूसरी औरत ‘नीमा’ थी और तीसरी ‘लोई’। नीमा कबीर के मस्तिष्क छायी रहती थी तो लोई हृदय के किसी कोने में रहती थी और माया हर जगह विद्यमान थी।”
 पेपरबैक
पेपरबैक
पृष्ठ: 160
मूल्य: 155 रुपए
प्रकाशक : एनबीटी, दिल्ली
समीक्षक : डॉ॰ रमा,
एसोसिएट प्रो॰, हिन्दी विभाग हंसराज कॉलेज, दिल्ली।
संप्रत्ति- कार्यवाहक प्राचार्य, हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
ईमेल: drrama1965@gmail.com
मो० : 09891172389
इस उपन्यास में कुछ ऐसे चरित्रों का भी उदघाटन किया है जो इतिहास के साँचे में नहीं आ सके। कबीर जिस तरह धर्मांधता में आकंठ डूबे भारतीय समाज को कड़े शब्दों में भक्ति का वास्तविक अर्थ समझा रहे थे उससे धर्म के ठेकेदारों को अवश्य बुरा लगा होगा। उनका संवाद और विवाद हजारों पाखंडी पंडितों और मौलवियों से हुआ होगा ही। ऐसा ही चरित्र मनसादेव का भी है। मनसादेव भैरव का भक्त था। मांस-मदिरा और स्त्री उसके प्रिय हैं। कबीर से उसकी टकराहट कई बार होती है जिसमें वह मनसादेव को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं परंतु वह अभिमानी और उदण्ड भी है। कबीर जब उसे आचरण की शुद्धता का उपदेश देते हैं तो उसका अभिमानी रूप जाग्रत हो उठता हैं। उसे कबीर बहुत तुच्छ व्यक्ति लगते हैं। कबीर ने कई स्थानों पर उससे संवाद किया अंततः वह कबीर की शरण में आ जाता है। उपन्यासकार ने ऐसे ही कुछ चरित्रों को चित्रित किया है जिसमें एक हंसा देव हैं।
प्रत्येक उपन्यास का एक ‘विजन’ होता है जिसे रचनाकार किसी न किसी संदर्भ में प्रस्तुत करता ही है। कैलाश नारायण तिवारी ने भी किया है। पूरे उपन्यास को पढ़ते हुए पहले से बनी कबीर की कई धारणाएँ तो टूटती ही हैं कई नई धारणाओं का जन्म भी होता है। यह पुस्तक सच में नए कबीर की खोज है। कबीर आजीवन आडंबरों और समाज द्वारा विकसित कर लिए गए धार्मिक बिसगतियों से परहेज ही नहीं किए बल्कि डंडा मारकर ठीक भी किया। उन्हे अपनी कविता को नहीं जीवन को दर्शन बनाना था। उपन्यासकार को यह बखूबी पता भी है। भले ही कल्पना की छूट लेकर ही सही पर कबीर के हवाले से एकदम सटीक लिखते है- “आशीर्वाद किसी को नहीं दूंगा। यहाँ तक की चेलों को भी नहीं। चमत्कारों से भी दूर रहूँगा। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन होगा। मेरी बातें ही साधना होंगी। मेरी वाणी ही लोगों के लिए मेरा संदेश होगा।”
सभी जानते हैं कबीर का जीवन का पहला अध्याय ही ‘गुरु’ की खोज से आरंभ होता है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है। आलोचकों से रामानन्द और कबीर के संबंध को बस यह कहकर ताल दिया है कि, काशी के मंदिर की किसी सीढ़ी पर लेते हुये कबीर पर रामानन्द का पैर पड़ जाता है और उनके मुँह से ‘राम’ शब्द का उच्चारण हो जाता है जिसे कभी मंत्र के रूप में स्वीकार कर लेते है। परंतु उपन्यासकर कुछ तथ्यों की तरह भी उन्मुख होता है । रामानन्द और कबीर के संबंध के कुछ और भी सूत्र खोलता है। वह लिखते हैं -“इतिहास और साहित्य इस बात पर चुप है कि कबीरदास गुरु रामानन्द के कितने करीब थे ? गुरु कि संगत में आने के बाद अपनी जिज्ञासाओं का या अपने प्रश्नों का निवारण वे किस सीमा तक कर पाये? दरअसल इस संबंध में कुछ थोड़े से सूत्र कबीर के पदों और दोहों में मिलते हैं। कबीर ने अनेक पदों और दोहों में गुरु कि महिमा का बखान किया है।” इस तरह देखें तो कई नई बात पता चलती है, जिसे रचनाकार ने बहुत ही सहजता से प्रस्तुत कर दिया है। इस उपन्यास में कई स्थानों पर कबीर की गुरु ढूँढने की व्याकुलता और छटपटाहट को रेखांकित किया है साथ ही कई जगहों पर उनका संवाद भी हुआ है जिसमें रामनन्द कबीर के ‘आंखिन देखी’ ज्ञान से विस्मित भी होते हैं और प्रसन्न भी। हिन्दी आलोचकों ने कबीर और रामानन्द के इस संबंध में कम ही चर्चा की है।
उपन्यासकार ने कबीर के महत्व को समझने के लिए उनका बकायदा अध्ययन किया है। हालाकि यह पुस्तक कबीर के ऊपर आलोचना नहीं है बल्कि उपन्यास है जिसमें रचनकर ने कई स्थानों पर कल्पना का सहारा लिया बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि कल्पना के माध्यम से कबीर का यथार्थ रच दिया है। वैसे भी यथार्थ के करीब पहुँचने के लिए कल्पना का सहारा लिया ही जाता है। लेकिन उपन्यास निरा-कल्पना भी नहीं है। रचनाकार ने जो तर्क दिया है और बात को जिस सलीके से रखा है वह कहीं भी भ्रमित नहीं करता है। कबीर के प्रादुर्भाव के संबंध में उन्होने एक स्थान पर लिखा है- “मध्यकालीन रूढ़िग्रस्त भारतीय समाज में सचमुच एक विचित्र। इतिहास ने समाज को एक ऐसा नायक, ऐसा योगी दे, एक ऐसा सत्यान्वेषी कवि दे दिया था जिसके पीछे चलने के लिए ढेर सारे लोग विवश हो गए थे। वह विवशता आगे चलकर इतिहास कि जरूरत भी बन गयी और क्षति-पूर्ति का साधन भी।” यह सच भी है। कबीर पूरी भक्ति कविता के ऐसे कबीर के रूप में चिन्हित हैं जिनकी काव्य चेतना जितनी प्रखर है स्वभाव भी उतना ही तेजस्वी है। वह बिसंगतियों पर कटाक्ष ही नहीं करते बल्कि उससे भिड़ भी जाते हैं। उनकी कविया की सबसे बड़ी विशेषता उसका विषय बद्ध न होना है साथ ही किसी एक भाषा और बोली बंधकर नहीं लिखना है। उन्होने अपनी कविता के लिए किसी एक विषय को नहीं चुना न किसी एक भाषा का चुनाव किया। हिन्दी के आलोचकों ने इसे एक कमी के रूप में भी देखने की कोशिश की पर देखना यह भी है की कबीर की कविता का फ़लक इसीलिए अन्य कवियों से बड़ा है। उनकी भाषा और विषय वस्तु नैतिक शिक्षा की तरह हैं जिसे अनपढ़ भी आसानी से समझ जाए और बौद्धिक भी चकरा जाए।
यह उपन्यास कई दृष्टियों से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हम पहली बार कबीर के चरित्र के अंदर तक प्रवेश कर पाते हैं। इतना ही नहीं कबीर के अन्तर्मन में छुपे उन रहस्यों से परिचित होते हैं जो कभी उनकी कविता में आसानी से नहीं देख पते हैं। अपने गहन अध्ययन से रचनाकार वहाँ तक पहुँचने में सफल हो जाता है। इसी संदर्भ में देखें तो कई स्थानों पर उपन्यासकार ने कबीर के प्रकृतिप्रेमी होने की चर्चा की है। एक स्थान पर उन्होने लिखा है कि- “कबीर प्राकृतिक उपदानों को जीवन की अमूल्य निधि मानते हैं क्योंकि प्रकृति से उनका निकट का संबंध था। पूरी-पूरी रात वह प्रकृति की गोद में बैठे बिता देते थे उस दिन भी बस एक ही बात लगातार सोचते रहे- ‘यह प्रकृति भी कितनी ममतामयी हैं। कितनी आनंददायिनी है। समान भाव से अपना सर्वस्व लुटा देती है; मनुष्य के ऊपर।” बहुत संभव है कि रचनाकर ने यहाँ पर भी कल्पना का सहारा लिया हो परंतु प्रकृति के प्रति कबीर के इस प्रेम-वर्णन में कहीं कोई अतिश्योक्ति नहीं झलकती है।
कबीर कि कविताओं में समाज ने अपनी पीड़ा तो ढूंढ ली गयी पर स्वयं उनका दुख: नहीं खोज पाया उपन्यासकार ने इस दिशा की तरफ भी ध्यान दिया है। उन्होने यह स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण भारतीय समाज को मानसिक बल देने वाली कबीर कि कविताओं में स्वयं उनके भी हृदय के उद्गार छुए हुए हैं। कबीर अपनी कविता में लगातार अपना दुख: व्यक्त कर रहे थे, बस उसे वह आम जनता से जोड़ देते थे जिससे लोग उसे सामाजिक मान लिया करते थे। रचनाकर ने लिखा है- “दुर्भाग्य से कम ही लोग जानते हैं कि कबीर का जीवन-संघर्ष उनकी कविता में निहित है जो हमेशा हमारी चेतना में गूँजती है। उनकी जीवन-यात्रा का सबूत स्वयं उनकी साखी, सबद रमैनी और पद हैं।”
सामयिक विमर्शों के केंद्र कबीर सबसे अधिक छाए रहे। चाहे वह दलित विमर्श हो या स्त्री विमर्श कबीर हर जगह याद किए जाते हैं। हिन्दी आलोचना में कबीर कि छवि स्त्री विरोधी ही व्यक्त कि गयी है। जहां वह नारी को बार-बार ‘माया महा ठगिनी’ कहते हैं। पर यह अंधूरा सच है। कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि उन्होने स्त्री का विरोध भी स्त्री कि रक्षा के लिए किया। उस समय स्त्री का मात्र भोग कि वस्तु समझा जाता था। चूंकि कबीर की वाणी का प्रभाव लाखों लोगों पर था इसलिए ‘माया’ कहते ही वह पुरुषों द्वारा भोग के दृष्टिकोण से मुक्त भी हो गयी होंगी। हलाकी यह विवाद का विषय हो सकता है परंतु इस उपन्यास को पढ़ते हुये यह महसूस होता है कि कबीर अपने माँ के बहुत करीब थे। यह पूरा उपन्यास ही कबीर से अपनी माँ नीमा से संवाद है। वह अपनी पत्नी लोई का भी आभार व्यक्त करते हैं। अपनी माँ और पत्नी का हद से ज्यादा आदर करने वाला व्यक्ति स्त्री विरोधी कैसे हो सकता है? इस प्रश्नों का जबाब बहुत तार्किकता से इस उपन्यास में मिल जाता है। रचनाकार ने कई स्थान पर इसका उदाहरण भी दिया है। यथा- “कबीर के जीवन में उन्हें सर्वाधिक प्रभावित करने वाली खास तौर पर तीन औरतें थीं। पहली औरत ‘माया’ थी जिसे जगत माता भी कह सकते हैं। दूसरी औरत ‘नीमा’ थी और तीसरी ‘लोई’। नीमा कबीर के मस्तिष्क छायी रहती थी तो लोई हृदय के किसी कोने में रहती थी और माया हर जगह विद्यमान थी।”
विरले दोस्त कबीर के
कैलाश नारायण तिवारी
 पेपरबैक
पेपरबैकपृष्ठ: 160
मूल्य: 155 रुपए
प्रकाशक : एनबीटी, दिल्ली
समीक्षक : डॉ॰ रमा,
एसोसिएट प्रो॰, हिन्दी विभाग हंसराज कॉलेज, दिल्ली।
संप्रत्ति- कार्यवाहक प्राचार्य, हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
ईमेल: drrama1965@gmail.com
मो० : 09891172389
इस उपन्यास में कुछ ऐसे चरित्रों का भी उदघाटन किया है जो इतिहास के साँचे में नहीं आ सके। कबीर जिस तरह धर्मांधता में आकंठ डूबे भारतीय समाज को कड़े शब्दों में भक्ति का वास्तविक अर्थ समझा रहे थे उससे धर्म के ठेकेदारों को अवश्य बुरा लगा होगा। उनका संवाद और विवाद हजारों पाखंडी पंडितों और मौलवियों से हुआ होगा ही। ऐसा ही चरित्र मनसादेव का भी है। मनसादेव भैरव का भक्त था। मांस-मदिरा और स्त्री उसके प्रिय हैं। कबीर से उसकी टकराहट कई बार होती है जिसमें वह मनसादेव को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं परंतु वह अभिमानी और उदण्ड भी है। कबीर जब उसे आचरण की शुद्धता का उपदेश देते हैं तो उसका अभिमानी रूप जाग्रत हो उठता हैं। उसे कबीर बहुत तुच्छ व्यक्ति लगते हैं। कबीर ने कई स्थानों पर उससे संवाद किया अंततः वह कबीर की शरण में आ जाता है। उपन्यासकार ने ऐसे ही कुछ चरित्रों को चित्रित किया है जिसमें एक हंसा देव हैं।
प्रत्येक उपन्यास का एक ‘विजन’ होता है जिसे रचनाकार किसी न किसी संदर्भ में प्रस्तुत करता ही है। कैलाश नारायण तिवारी ने भी किया है। पूरे उपन्यास को पढ़ते हुए पहले से बनी कबीर की कई धारणाएँ तो टूटती ही हैं कई नई धारणाओं का जन्म भी होता है। यह पुस्तक सच में नए कबीर की खोज है। कबीर आजीवन आडंबरों और समाज द्वारा विकसित कर लिए गए धार्मिक बिसगतियों से परहेज ही नहीं किए बल्कि डंडा मारकर ठीक भी किया। उन्हे अपनी कविता को नहीं जीवन को दर्शन बनाना था। उपन्यासकार को यह बखूबी पता भी है। भले ही कल्पना की छूट लेकर ही सही पर कबीर के हवाले से एकदम सटीक लिखते है- “आशीर्वाद किसी को नहीं दूंगा। यहाँ तक की चेलों को भी नहीं। चमत्कारों से भी दूर रहूँगा। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन होगा। मेरी बातें ही साधना होंगी। मेरी वाणी ही लोगों के लिए मेरा संदेश होगा।”
००००००००००००००००
















