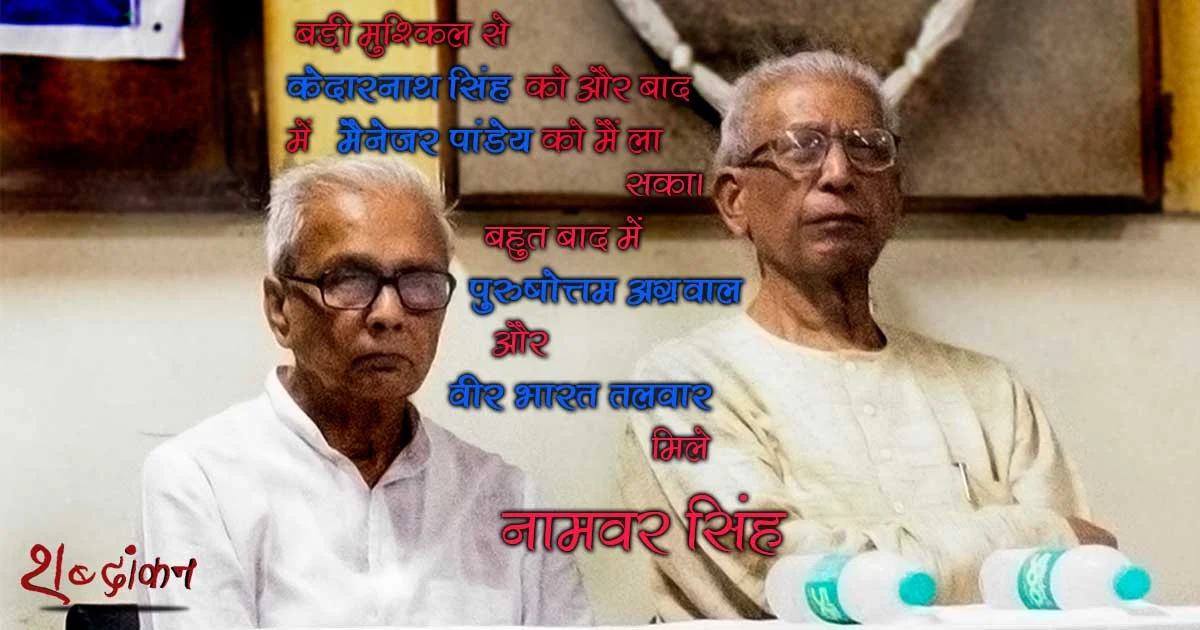
Jeevan kya Jiya - 5
Namvar Singh
जीवन क्या जिया!
(नामवर सिंह लिखित आत्मकथा का अंश)
हिन्दी का गढ़ तो दिल्ली है, इलाहाबाद है, बनारस है
कुल मिला कर मैं सन् 52 से 92 तक अध्यापक रहा। इसमें से पाचं साल मेरी बेकारी के और पांच साल गैर अकादमिक काम के निकाल दिये जायें तो कुल तीस साल मैंने विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और शिक्षक रहा। काशी हिन्दू वि.वि. में पढ़ाने का अपना आनंद था। शोध कार्य करते समय ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। वहां मैं मुख्यतः बी.ए. में कामर्स और विज्ञान के गैर साहित्यिक विद्यार्थियों को सामान्य हिन्दी पढ़ाता था। एम.ए. में आरम्भ में अपभ्रंश और बाद में भाषा विज्ञान पढ़ाता था। एक तरफ अपभ्रंश और भाषा विज्ञान जैसे नीरस विषय, तो दूसरी तरफ सामान्य हिन्दी के नाम पर एक कहानी संग्रह तथा एक गद्य संकलन जैसा कुछ होता था। जो कोई नहीं पढ़ाना चाहता था वह मुझे पढ़ाने को मिला था। लेकिन अध्यापन के मेरे सर्वाधिक सुखद क्षण काशी हिन्दू वि.वि. के ही हैं। किताबें तो बहाना होती हैं, खूंटी हैं जिन पर आप कोई भी कपड़ा टांग सकते हैं। मेरी दिलचस्पी यह थी कि विद्यार्थियों में रुचि पैदा हो, कहानी के प्रति, कविता के प्रति, भाषा के प्रति, गद्य के प्रति। मेरी किताब बकलमखुद उन्हीं दिनों छपी थी। इस पुस्तक के निबंधों की फक्कड़ाना मस्ती वाली शैली में मैं अध्यापन किया करता था। और मैंने पाया कि कमरा विद्यार्थियों से ठसाठस भरा रहने लगा था। सीट पर जगह नहीं रहती थी। तमाम लोग खड़े रहते थे, यहां तक कि क्लास के बाहर खड़े होकर सुनते थे। दरअसल दूसरी कक्षाओं, यहां तक कि शहर के कुछ कालेजों के विद्यार्थी भी आने लगे थे। दरवाजों खिड़कियों पर ठसे हुए विद्यार्थी। भयंकर भीड़ रहती थी। उधर से गुजरते हुए लोग कहते थे, ”यह कौन है भई, क्या पढ़ा रहा है?“ एक साहब जल भुन कर बोले थे, ”ही मस्ट बी टाकिंग समथिंग पापुलर।“ यह वाक्य मेरे कान में पड़ा। यह सुख था हमारा।
हालांकि जीवन में अभाव और दुख थे। उन दिनों हमारी हालत यह थी कि एक ही कुर्ता था, उसी को धोकर, सुखा कर, पहन कर मैं आया करता था। वजीफा मिल नहीं रहा था, डे हास्टल में रहता था। ये करीब नौ दस महीने थे। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मेस में मुफ्त खाने की व्यवस्था हो गयी थी। पैदल चलता था। लेकिन मेरे उत्साह में कमी न थी। अध्यापन के वे बेहतरीन अनुभव थे और वैसा सुख जीवन में उसके बाद नहीं मिला। साथ ही मैंने वहां पाठ्यक्रम बदलने में पंडित जी की मदद की। वह शांतिनिकेतन से आये थे और पाठ्यक्रम को लेकर उनके और मेरे कुछ मिलनबिन्दु थे, वे बड़े समान थे। मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था, ”भाई देखो, जयशंकर प्रसाद तो यहां ‘आलू’ हैं। उनकी कविताएं पढ़ो, उन्हीं का उपन्यास पढ़ो, उनकी कहानी भी पढ़ो।“ उन्होंने उपन्यास और कहानी में प्रेमचंद को विशेष महत्व देने की बात की थी। सागर जाने पर बनारस का सुख छूट गया। हालांकि अशोक वाजपेयी से पता चलेगा कि सागर में भी मेरी कक्षा में दूसरे अध्यापकों के विद्यार्थी आकर बैठ जाते थे। वहां भी बनारस की थोड़ी हवा पहुंची थी। लेकिन बस इतना ही। सागर विश्वविद्यालय में कुछ बौद्धिक मित्र मिले जैसे दयाकृष्ण और श्यामाचरण दुबे। साहित्यिक मित्रों में विजय चौहान, प्रबोध कुमार, आग्नेय, नईम और अशोक।
हां जोधपुर में मैं इस स्थिति में था कि विश्वविद्यालय में हिन्दी को लेकर जो मेरा नक्शा था, उसे लागू कर सकूं। ‘आलोचना’ का मैं एक अंक निकाल चुका था वि.वि. में हिन्दी शिक्षा। तो मैंने पाया कि मैं बनारस में भी जो नहीं कर सका, वह करने का मौका जोधपुर में है। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मैं जोधपुर में रह कर बदलाव की कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन हिन्दी का गढ़ तो दिल्ली है, इलाहाबाद है, बनारस है। दिल्ली स्थित जे.एन.यू. का प्रस्ताव स्वीकार करने के पीछे मेरी इस सोच का भी बहुत बड़ा हाथ था। सचमुच काम करने की असली जगह मुझे जे.एन.यू. में मिली। यहां मैंने साफ पटिया पर शुरू किया था जिस पर पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं था। इस विश्वविद्यालय का ढांचा स्कूल आफ सोशल साइंसेज का था। वामपंथी विचारों का वर्चस्व भी था। सब कुछ अनुकूल था लेकिन काम करने के लिए सहयोगियों की भी जरूरत होती है। मैंने हिन्दी उर्दू को साथ रखा था और मुझे खुशी है कि मुझे बहुत अच्छे सहयोगी मिले लेकिन यह बाद की बात है। जब मैं यहां आया था तो विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष सतीश चंद्र की पत्नी शोभा जी थीं। और एक सुधेश जी थे। तो हमें दो ‘स’ मिले थे। दोनों ही शोभा थे, कुछ हो नहीं सकता था और नयी पोस्ट मिल नहीं रही थी लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी। प्रोफेसर बी.डी. नाग चौधरी वी.सी. थे। उनके भाई काशी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। बनारस में उनके पिताजी हमारे प्रिन्सिपल रह चुके थे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से केदारनाथ सिंह को और बाद में मैनेजर पांडेय को मैं ला सका। बहुत बाद में पुरुषोत्तम अग्रवाल और वीर भारत तलवार मिले।
मैं जब जे.एन.यू.पहली बार पहुंचा था तो कोई हिन्दी बोलने वाला नहीं मिलता था। अंगे्रजी का वर्चस्व था। मैंने पाया कि एक हिन्दी विमुख समाज में हिन्दी को स्थान दिलाना है। विचित्र स्थिति थी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में तो बड़े ऊंचे ऊंचे लोग थे लेकिन हिन्दी में वैसी समृद्धि नहीं थी। मैंने निश्चय किया कि यहां हिन्दी को ऐसे स्तर पर पहुंचा देना है कि देख कर लगे कि हां यह जे.एन. यू. का विद्यार्थी है। इसके लिए सबसे पहले उसमें स्वाभिमान भरना था। उसके भीतर से यह हीनता ग्रंथि निकाल बाहर करनी थी कि वह इतिहास, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की तुलना में किसी भी तरह से कम है।
जे.एन.यू. में खाली पाठ्यक्रमों की कूपमंडूकता तोड़ने का ही प्रश्न नहीं था। यह सिद्ध करना भी जरूरी था कि वहां का जो बौद्धिक स्तर है, उस स्तर पर हिन्दी के अध्यापक और विद्यार्थी दिखायी पड़ें। ऐसा न हो कि अन्य विभाग के अध्यापक तो प्रोफेसर लगें और हिन्दी के अध्यापक प्राइमरी के मास्टर लगें। मुझे संतोष है कि हमारे सेण्टर ने बहुत जल्द दिखा दिया कि किसी से हम नीचे नहीं हैं। जिस सेण्टर में केदारनाथ सिंह जैसा कवि, मैनेजर पांडेय जैसा आलोचक और विचारक हो, पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसा तेजस्वी बौद्धिक हो, वीर भारत तलवार जैसा गम्भीर खोजी हो, वह उपेक्षणीय नहीं हो सकता।
संयोग से प्रो. मूनिस रजा रेक्टर थे और देवी प्रसाद त्रिपाठी छात्रसंघ के अध्यक्ष। एक गाजीपुरी दूसरा सुल्तानपुरी। हिन्दी के अधिसंख्य छात्र भी पूरब के थे। विश्वविद्यालय में पुरवा हवा के साथ हिन्दी फैलने लगी। एक हवा बह रही थी जैसे। हिन्दी के लड़के छात्रसंघ के अध्यक्ष बने आगे चल कर। साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हिन्दी में होने लगे।
लेकिन यहां पढ़ाने का दूसरा अनुभव था। यहां कक्षाएं छोटी होती थीं। बीस विद्यार्थी रहते थे। काशी हिन्दू वि.वि. में चार सौ के सामने भाषण दे रहे होते थे और यहां बीस के सम्मुख बातचीत करनी थी। अब बीस लोगों की मंडली में गोष्ठी करने के दिन आ गये थे। विद्यार्थी भी एम.ए. और एम.फिल. के। कोर्स भी बिलकुल नये नये। बौद्धिक चुनौती महसूस होती थी। इसका मजा कुछ और ही था।
मैं यह कभी नहीं भूला कि मैं एक प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा हूं और जब तक मैं वि.वि. के अलावा स्कूली शिक्षा के लिए कुछ नहीं करता, पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मुझे ऐसा मौका मिला एनसी. ई.आर.टी. के जरिये। उस जमाने में प्रोफेसर रईस अहमद डायरेक्टर होकर आये थे और प्रोफेसर नूरुल हसन शिक्षा मंत्री थी। ये सन् 1972-73 के दिन थे। तय हुआ था कि नये ढंग की पाठ्य पुस्तकें तैयार करायी जायें। इसके लिए जो कमेटी बनी उसमें मैं भी था। आगे चल कर मैं पाठ्य पुस्तक समिति का अध्यक्ष भी हुआ। मैंने जो नये ढंग की पुस्तकें तैयार करायीं, उनसे पाठ्यक्रम बदल गया। अब एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम में नागार्जुन का उपन्यास नयी पौध था। भैरव जी के गंगा मैया को रखा गया। कहानी संकलन जो तैयार कराया उसमें ज्ञानरंजन की, काशी की कहानियां थीं। कविता में धूमिल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह आदि की कविताएं हमने रखीं। पहले एन.सी.ई.आर.टी. में डा. नगेन्द्र और विजेन्द्र स्नातक का राज था वह युग समाप्त हुआ। हिन्दी साहित्य का नया इतिहास डा. विश्वनाथ त्रिपाठी से लिखवाया। संक्षिप्त इतिहास। लोगों को मालूम है कि केन्द्रीय विद्यालयों और पब्लिक स्कूलों में यही कोर्स चलता है, यही किताबें पढ़ी पढ़ायी जाती हैं। जब मैं स्वयं कमेटी का अध्यक्ष हुआ तो हिन्दी के जीवित महत्वपूर्ण लेखकों पर फिल्में बनवायीं। नागार्जुन, हरिशंकर परसाई, शिवमंगल सिंह ‘सुमन’, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह आदि पर फिल्में बन चुकी हैं एक लम्बी योजना है हमारी।
वैसे तो मुख्यतः मेरा क्षेत्र वि.वि. है। स्कूलों में मैंने पढ़ाया नहीं, कोई अनुभव नहीं फिर भी मैंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल की। दरअसल स्कूल से लेकर वि.वि. तक हिन्दी के पाठ्यक्रम को बदलना जरूरी है, और इस दिशा में मैंने ईमानदारी से पूरी कोशिश की। क्योंकि इन्हीं संस्थाओं से लेखक पैदा होते हैं, पाठक पैदा होते हैं। ये बदल जायें तो हिन्दी साहित्य का पूरा माहौल बदल सकता है।
क्रमशः...
००००००००००००००००

















1 टिप्पणियाँ
Nice Thanks For Sharing
जवाब देंहटाएं